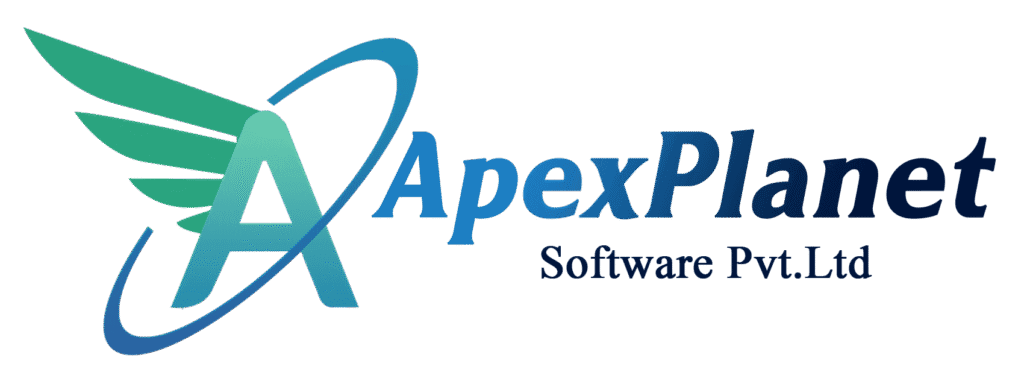नवीकरणीय ऊर्जा (Navikarniya Urja)

इस Editorial में The Hindu, The Indian Express, Business Line आदि में प्रकाशित लेखों का विश्लेषण किया गया है। इस लेख में Navikarniya Urja और उसके महत्त्व पर चर्चा की गई है। साथ ही भारत में उसकी स्थिति और मौजूदा चुनौतियों का भी उल्लेख किया गया है। आवश्यकतानुसार, यथास्थान टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल किये गए हैं।
संदर्भ
ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों मुख्यतः जीवाश्म ईंधन की खोज ने मानव इतिहास के विकास को एक नई दिशा दी। उल्लेखनीय है कि जीवाश्म ईंधन में कई सौ वर्षों तक पूरी दुनिया की ऊर्जा मांगों को पूरा करने की क्षमता है। इसने बीसवीं शताब्दी में हुई औद्योगिक क्रांति में भी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। परंतु दुनिया भर में इसकी अत्यधिक खपत ने कई चुनौतियों को भी जन्म दिया जिसके कारण दुनिया इसके प्रतिस्थापन के बारे में सोचने को मजबूर हो गई। 1970 के दशक में पर्यावरणविदों ने जीवाश्म ईंधन से हमारी निर्भरता को कम करने और उसके प्रतिस्थापन के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना शुरू किया। 21वीं सदी की शुरुआत में दुनिया की ऊर्जा खपत का 20 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त होने लगा था। ध्यातव्य है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने भी अपनी बिजली उत्पादन क्षमता का काफी विस्तार किया है। विगत तीन वर्षों में नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा में लगभग 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों मुख्यतः जीवाश्म ईंधन की खोज ने मानव इतिहास के विकास को एक नई दिशा दी। उल्लेखनीय है कि जीवाश्म ईंधन में कई सौ वर्षों तक पूरी दुनिया की ऊर्जा मांगों को पूरा करने की क्षमता है। इसने बीसवीं शताब्दी में हुई औद्योगिक क्रांति में भी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। परंतु दुनिया भर में इसकी अत्यधिक खपत ने कई चुनौतियों को भी जन्म दिया जिसके कारण दुनिया इसके प्रतिस्थापन के बारे में सोचने को मजबूर हो गई। 1970 के दशक में पर्यावरणविदों ने जीवाश्म ईंधन से हमारी निर्भरता को कम करने और उसके प्रतिस्थापन के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना शुरू किया। 21वीं सदी की शुरुआत में दुनिया की ऊर्जा खपत का 20 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त होने लगा था। ध्यातव्य है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने भी अपनी बिजली उत्पादन क्षमता का काफी विस्तार किया है। विगत तीन वर्षों में नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा में लगभग 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
क्या होती है नवीकरणीय ऊर्जा?
Navikarniya Urja ऐसी ऊर्जा है जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है। इसमें सौर ऊर्जा, भू-तापीय ऊर्जा, पवन, ज्वार, जल और बायोमास के विभिन्न प्रकारों को शामिल किया जाता है।
उल्लेखनीय है कि यह कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है और इसे लगातार नवीनीकृत किया जाता है।
नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों (जो कि दुनिया के काफी सीमित क्षेत्र में मौजूद हैं) की अपेक्षा काफी विस्तृत भू-भाग में फैले हुए हैं और ये सभी देशों को काफी आसानी हो उपलब्ध हो सकते हैं।
ये न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं बल्कि इनके साथ कई प्रकार के आर्थिक लाभ भी जुड़े होते हैं।
Navikarniya Urja में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है:
वायु ऊर्जा
सौर ऊर्जा
हाइड्रोपावर
बायोमास
जियोथर्मल
नवीकरणीय ऊर्जा (Navikarniya Urja)का महत्त्व
नवीकरणीय ऊर्जा (Navikarniya Urja)पर्यावरण के अनुकूल है
यह ऊर्जा का एक स्वच्छ स्रोत है, अर्थात् इसमें न्यूनतम या शून्य कार्बन और ग्रीनहाउस उत्सर्जन होता है। जबकि इसके विपरीत जीवाश्म ईंधन ग्रीनहाउस गैस और कार्बन डाइऑक्साइड का काफी अधिक उत्सर्जन करते हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और वायु की गुणवत्ता में गिरावट के लिये काफी हद तक ज़िम्मेदार हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधन वायुमंडल में सल्फर का भी उत्सर्जन करते हैं जिसके प्रभाव से अम्लीय वर्षा होती है। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को काफी कम करता है।
ऊर्जा का स्थायी स्रोत
नवीकरणीय (Navikarniya Urja)संसाधनों से प्राप्त ऊर्जा को ऊर्जा का स्थायी स्रोत माना जाता है, इसका तात्पर्य यह है कि वे कभी भी समाप्त नहीं होते हैं या कह सकते हैं कि उनके खत्म होने की संभावना लगभग शून्य होती है। वहीं दूसरी ओर जीवाश्म ईंधन (तेल, गैस और कोयला) जैसे ऊर्जा के स्रोतों को सीमित संसाधन माना जाता है और इस बात की प्रबल संभावना होती है कि वे भविष्य में समाप्त हो जाएंगे।
रोज़गार सृजन में सहायक(Navikarniya Urja)
नवीकरणीय ऊर्जा (Navikarniya Urja)अन्य परंपरागत विकल्पों की अपेक्षा एक बेहतर और सस्ता स्रोत है। ध्यातव्य है कि जैसे-जैसे विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा(Navikarniya Urja) का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, नए और स्थायी रोज़गारों का भी निर्माण होता जा रहा है। उदाहरण के लिये जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिये कई नए रोज़गारों का सृजन हुआ है।
वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में स्थिरता(Navikarniya Urja)
नवीकरणीय ऊर्जा (Navikarniya Urja) को प्रोत्साहन दिये जाने से दुनिया के कई देशों में इसका काफी बढ़ चढ़ कर प्रयोग हो रहा है जिसके कारण वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में काफी स्थिरता आई है।
सार्वजानिक स्वास्थ्य को बढ़ावा
कई अध्ययनों में यह सामने आया है कि नवीकरणीय ऊर्जा (Navikarniya Urja) और लोगों के स्वास्थ्य में सीधा संबंध होता है और सरकारें ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों पर जो भी निवेश करती हैं उसका स्पष्ट प्रभाव आम लोगों के स्वास्थ्य स्तर में देखने को मिलता है। ध्यातव्य है कि जीवाश्म ईंधन द्वारा उत्सर्जित ग्रीनहाउस, कार्बन और सल्फर आदि मानव स्वास्थ्य के लिये काफी हानिकारक होते हैं।
प्रतिस्थापन की आवश्यकता क्यों?
यद्यपि तेल, प्राकृतिक गैस और कोयला प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु जिस खतरनाक दर से इनका उपभोग किया जा रहा है उससे यह स्पष्ट है कि एक दिन वे अवश्य ही खत्म हो जाएंगे।
इसके अतिरिक्त इन्हें अल्पकाल में पुनः प्राप्त करना भी संभव नहीं है, क्योंकि इस प्रक्रिया में लाखों वर्षों से भी अधिक समय लगता है।
जीवाश्म ईंधन से ग्रीनहाउस गैसों जैसे- मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि का उत्सर्जन होता है, जो ओज़ोन परत को नुकसान पहुँचाने में सक्षम हैं।
जीवाश्म ईंधन के निष्कर्षण ने कुछ क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन को खतरे में डाल दिया है। इसके अलावा कोयला खनन ने कई खदान श्रमिकों के जीवन को खतरे में डाल दिया है।
वर्तमान में जीवाश्म ईंधन का निष्कर्षण भी काफी महँगी प्रक्रिया हो गई(Navikarniya Urja), जिसके कारण उनकी कीमतों पर काफी असर पड़ा है।
जीवाश्म ईंधन का परिवहन काफी जोखिमपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इनके रिसाव से गंभीर खतरे पैदा हो सकते हैं।
ये ग्लोबल वार्मिंग में काफी ज़्यादा योगदान देते हैं।
भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थिति
स्वच्छ पृथ्वी के प्रति ज़िम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए भारत ने संकल्प लिया है कि वर्ष 2030 तक बिजली उत्पादन की हमारी 40 फीसदी स्थापित क्षमता ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों पर आधारित होगी।(Navikarniya Urja)
साथ ही यह भी निर्धारित किया गया है कि वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी। इसमें सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट, बायो-पावर से 10 गीगावाट और छोटी पनबिजली परियोजनाओं से 5 गीगावाट क्षमता प्राप्त करना शामिल है।
इस महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के साथ ही भारत विश्व के सबसे बड़े स्वच्छ ऊर्जा उत्पादकों की कतार में शामिल हो जाएगा। यहाँ तक कि वह कई विकसित देशों से भी आगे निकल जाएगा।
वर्ष 2018 में देश की कुल स्थापित क्षमता में तापीय ऊर्जा की 63.84 फीसदी, नाभिकीय ऊर्जा की 1.95 फीसदी, पनबिजली की 13.09 फीसदी और नवीकरणीय ऊर्जा की 21.12 फीसदी हिस्सेदारी थी।
क्या हैं चुनौतियाँ?
जीवाश्म ईंधन की अपेक्षा नवीकरणीय संसाधनों से अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करना अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। जीवाश्म ईंधन से आज भी बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन हो रहा है, जो स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि नवीकरणीय ऊर्जा अभी भी उतनी सक्षम नहीं है कि वह पूरे देश की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कर सके।
नवीकरणीय संसाधनों से ऊर्जा उत्पादन पूर्णतः मौसम और जलवायु पर निर्भर करता है तथा यदि मौसम ऊर्जा उत्पादन के अनुकूल नहीं होगा तो हम आवश्यकतानुसार ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर पाएंगे।
नवीकरणीय ऊर्जा (Navikarniya Urja)प्रौद्योगिकियाँ बाज़ार में अभी भी काफी नई हैं जिसके कारण उनके पास आवश्यक दक्षता की कमी है।
नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु सरकारी प्रयास
जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन
जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत 11 जनवरी, 2010 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। इस मिशन के तहत वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा के उत्पादन का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वर्ष 2015 में भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक भारत की सौर ऊर्जा क्षमता लक्ष्य को पाँच गुना तक बढ़ाने के लिये अपनी स्वीकृति दी, जो कि 1,00,000 मेगावाट हो गया है।
राष्ट्रीय बायोगैस और खाद प्रबंधन कार्यक्रम
राष्ट्रीय बायोगैस और खाद प्रबंधन कार्यक्रम एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। इसके तहत देश के ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्र के घरों में खाना पकाने के ईंधन और प्रकाश के स्रोत के रूप में बायोगैस गैस को प्रोत्साहित करने के लिये एक बायोगैस संयंत्र की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
सूर्यमित्र कार्यक्रम
इस कार्यक्रम की शुरुआत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान द्वारा की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्पन्न हो रहे नए अवसरों को देखते हुए इस क्षेत्र में युवाओं को कौशल प्रदान करना है। सूर्यमित्र कार्यक्रम युवाओं को सौर ऊर्जा क्षेत्र में नए उद्यमी बनने के लिये भी तैयार करता है।
सौर ऋण कार्यक्रम (Navikarniya Urja)
इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी और मात्र तीन वर्षों में लगभग 16,000 से अधिक सोलर होम सिस्टम को 2,000 बैंक शाखाओं के माध्यम से वित्तपोषित किया गया है। इस कार्यक्रम ने विशेष रूप से दक्षिण भारत के उन ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य किया जहाँ पर तब तक बिजली नहीं पहुँची थी।
क्या किया जाना चाहिये
उल्लेखनीय है कि एक थर्मल प्लांट की प्रति मेगावाट औसत लागत सौर संयंत्र की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत कम है। थर्मल प्लांट विशाल क्षमता के होते हैं और एक थर्मल प्लांट औसतन 18 सौर या पवन प्लांट के समान ही बिजली उत्पन्न करता है। इसलिये गैर-जीवाश्म स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने हेतु भविष्य में बड़े सौर और पवन संयंत्रों का निर्माण किया जाना आवश्यक है ताकि वे थर्मल प्लांट के समान कार्य कर सकें।
आँकड़े दर्शाते हैं कि बीते दो दशकों में कुल उत्पादन क्षमता का 63 प्रतिशत निजी क्षेत्र से आया है। अतः यह स्पष्ट है कि यदि देश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है तो निजी क्षेत्र को निवेश हेतु अधिक-से-अधिक प्रेरित करना होगा।(Navikarniya Urja)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.